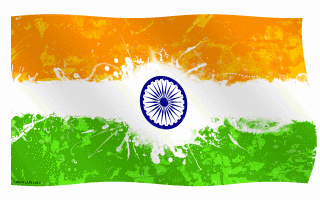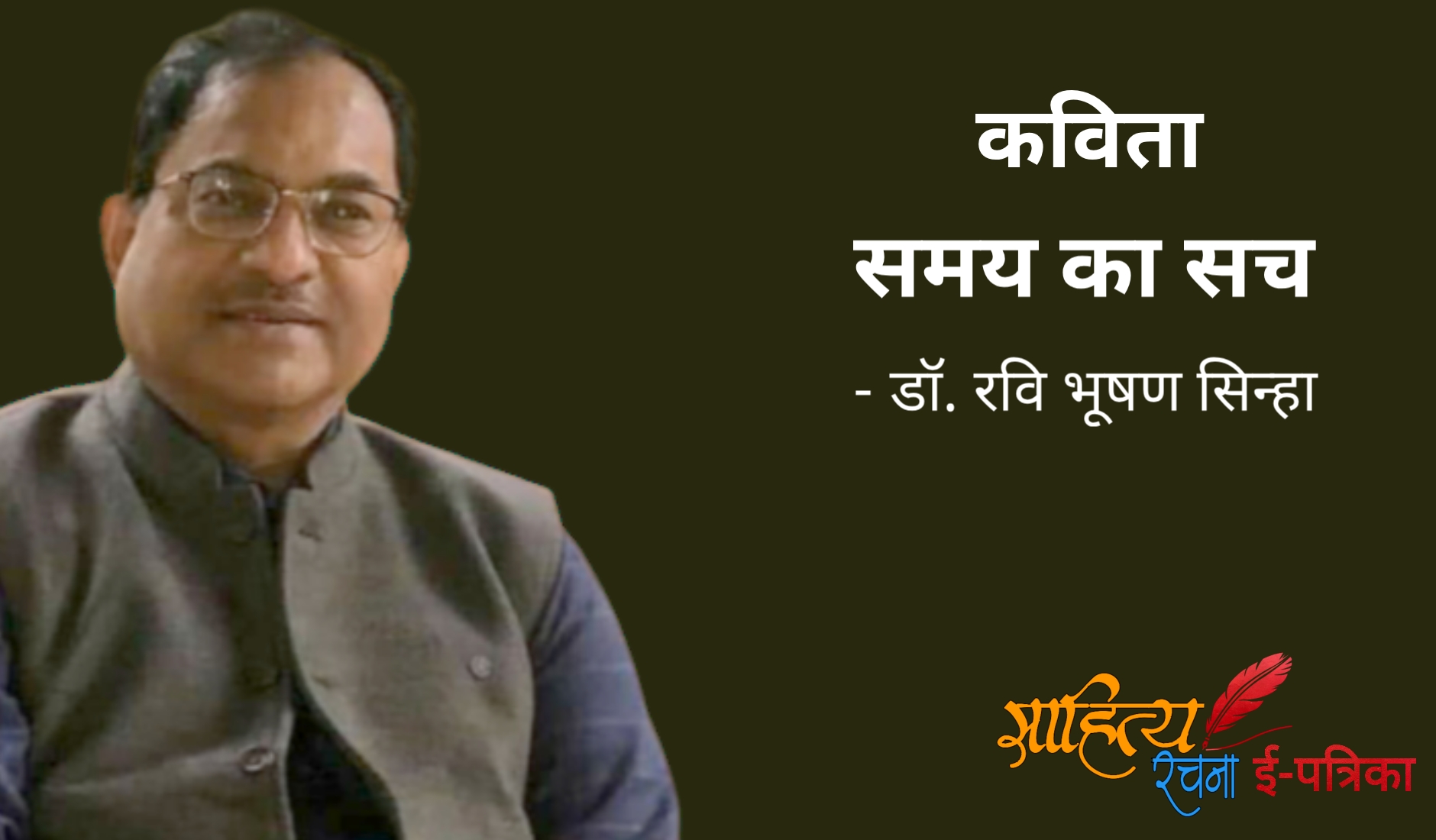जब-जब गरजा मुझ पर,
कुम्हार की अनुभूति से पीड़ित,
चमक देने का था मुक्त अंदाज,
कुछ माया का लगता था जाल।
कुछ पाकर भी था बेहाल।
कभी बूंदें थी आँखो में,
कभी डर था झुकने में,
मन में झूठी आशा लिए,
बापू से सच की परिभाषा लिए,
बेबस था घर लगती माँ की मार।
जीवन था कुछ दुनियां पार।
एक तरफ डंडे का जोर,
ऊपर से फिर गणित कमजोर,
भाग-भाग में बस रहा भाग में,
विचित्र थी ये जोड़-घटा,
फिर होता चाटा, मेरा गाल।
कुछ पाकर भी था बेहाल।
हमदर्दी हां शर्मंदगी को मात देती,
भले अनपढ़ की दिवार था मैं,
मुझको तराशने में कोई कमी तो न थी,
खुदगर्ज था बस महज़ खेल में,
कुछ वर्ष था बस उनकी जेल में।
लगता अब तुम बिन जी ना सकूँ,
कैसे अद्भुत गुरुवर इतिहास लिखूँ?
कुछ खोकर आया अब भूचाल,
कुछ पाकर भी था बेहाल।
मयंक कर्दम - मेरठ (उत्तर प्रदेश)