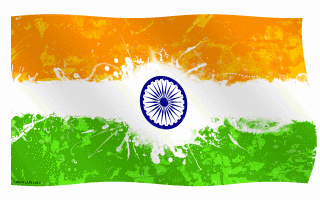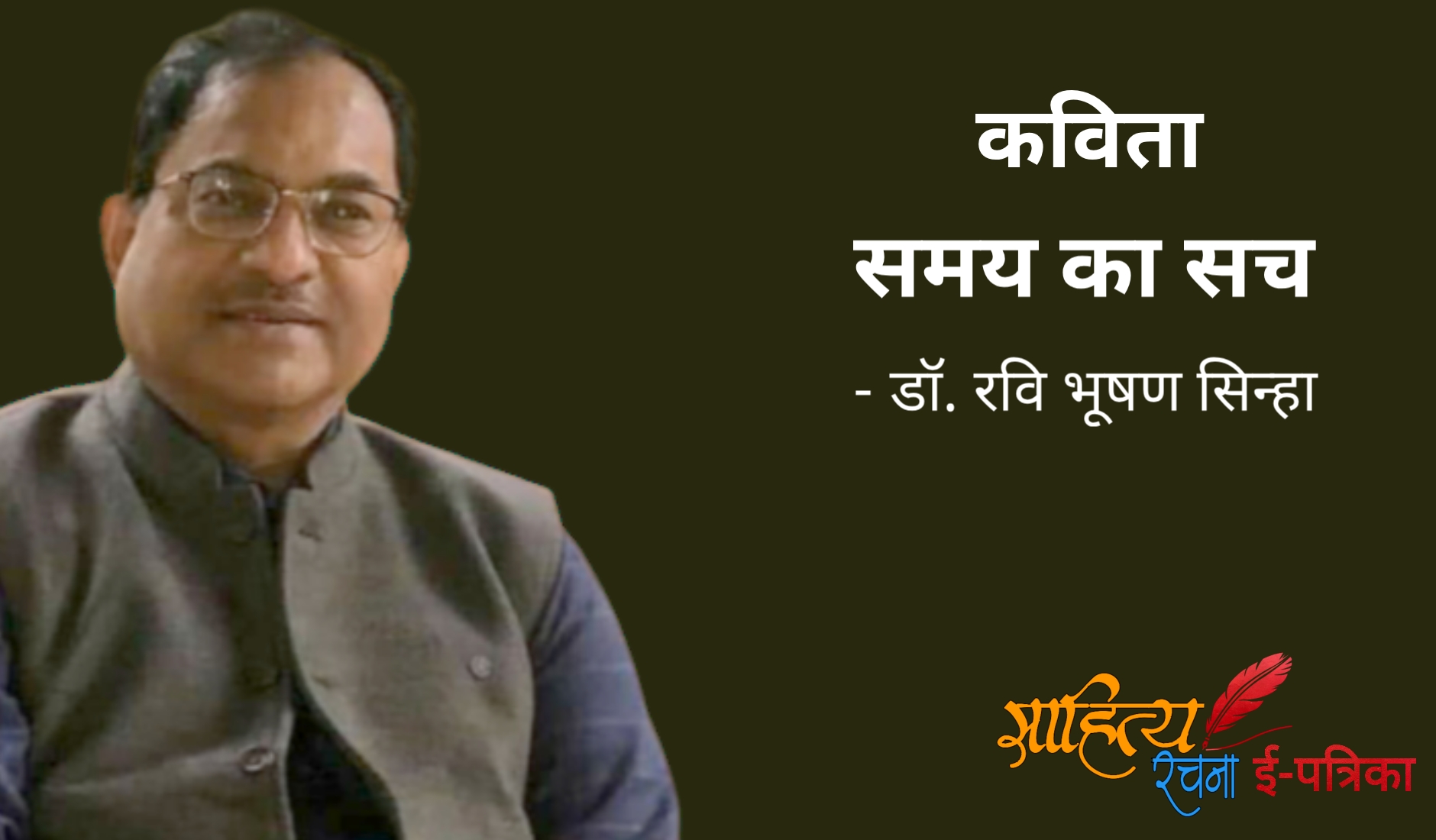सुषमा दीक्षित शुक्ला - राजाजीपुरम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
रेत - कविता - सुषमा दीक्षित शुक्ला
मंगलवार, अप्रैल 27, 2021
रेत सा फिसलता रहता,
बेदर्द वक़्त बंद मुट्ठी से,
फिर भी मन में है मचलती,
आसमान की सी उमंगे।
रेत के टीले सी उन्मुक्त,
ढहती हुई ज़िंदगानी,
फिर भी मानव की उम्मीदी देखो।
बस एक मुट्ठी देह में ही,
ये आकाश जैसे मन सँवरते।
नैनों की नन्ही सी कोठरी में
गगनचुंबी ख़्वाब पलते।
रेत तू तो रेत ही ठहरी न,
कब बन सके हैं तेरे महल।
एक तिनका उड़ा देता है तेरा वजूद।
फिर भी तेरे मीलों लम्बे ऊँचे गुंबद।
जगाते हैं एक अजीब सी उम्मीद।
हवा के साथ उड़कर,
ऊँचाई को छू लेने की तेरी जिजीविषा।
शायद यही है जीवन व्यथा,
यही है तेरी मेरी कहानी भी।
तेरी यही मौन अभिव्यक्ति
यही है संवेदना तेरी।
और तेरे हौसले की उड़ान भी।
तेरा वजूद है कितना नाज़ुक,
और कितना शक्तिशाली भी,
जब तू अपने बवंडर से,
ले उड़ती है पूरी की पूरी बस्तियाँ।
परन्तु ये भी बदनसीबी ही है
रेत के घर सजाने वालों की।
कि जब जब जगी उम्मीद,
कोई जलजला बहा ले गया,
रेत का घर हो महल।
ज़िंदगी सी मचल कर
रह जाती है किसी की मासूमियत
फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती दामन।
फिर से तलाशती है जीवन।
शायद यही है मंथन,
यही है यही दर्शन जीवन दर्शन।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर