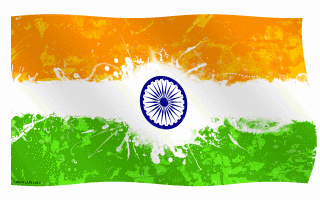बसंत हमारी आत्मा का गीत और मन के सुरों की वीणा है - लेख - सुनीता भट्ट पैन्यूली
गुरुवार, जनवरी 26, 2023
जनवरी का महीना था ज़मीन से उठता कुहासा मेरे घर के आसपास विस्तीर्ण फैले हुए गन्ने के खेतों पर एक वितान सा बुनकर मेरे भीतर न जाने कहीं सहमे हुए बच्चे की तरह बुझा-बुझा सा बैठ जाया करता था।
लाख चेष्टा की मैंने मेरे भीतर बैठ गए डरे सहमे से उस कुहासे रूपी बच्चे को माघ की बहुरूपिया धूप में धुपियाने की किंतु वह ठगनी धूप मेरे भीतर बैठे उदास बच्चे की अन्यमनस्कता को कभी पढ़ ही नहीं पाई, न ही सहला पाई हौले से उसकी बेजान पड़ी दिल की झंकारों को किसी संगीत के सुर में ढालकर।
मेरे घर के हाते में एक विचित्र सा पेड़ लगा है बारीक सी बुझी-बुझी सी पत्तियों वाला। माघ के भीषण कोहरे में न चाहते हुए भी उसकी मलिनता, काहिली पत्तियों से छनकर मेरे संपूर्ण अस्तित्व में घर कर जाती है मन आया उस गाछ को उखाड़ कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूँ किंतु प्रकृति से ही अथाह स्नेह रखने वाली मैं मुझसे यह नहीं हो पाया, छोड़ दिया उसे मैंने अपने जीवन के प्रवाह में स्वच्छंद बहने हेतु। किसी ने बताया यह तोर की दाल का पेड़ है (तोर की दाल उत्तराखंड के पहाड़ी खान-पान का अहम हिस्सा है)
जनवरी चली गई है हौले से फ़रवरी ने बसंत का आग़ाज़ किया है, किसलयों ने मुस्कराकर सुना है भौंरों का बेचैन राग हौले से, पंखुड़ियाँ फैलाकर वह पुष्प में कब परिणत हो जाएँगी यह उन्हें भी अहसास नहीं होगा क्योंकि बसंत की बयार चहुँओर है चर-अचर लालायित हैं प्रेम में पगा होने के लिए।
मेरे खेत की मेड़ों पर उमग आए हैं भाकले के पेड़, पीली सरसों, मटर की हरहराती बेलें, फ्यूली के फूलों से रहगुज़र मेरे दृग भी प्रकृति प्रदत्त बसंत पर निसार होने लगे हैं।
वह तोर की दाल का पेड़ याद है न आपको जनवरी के महीने का उदासी भरा पेड़? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है बसंत का यौवन उस पर टूट कर बरस पड़ा है इतना ख़ूबसूरत जैसे कि सेहरा पहने दूल्हा धरा से परिणय सूत्र में बंधने जा रहा हो।
बसंत उस तोर के पेड़ पर आएगा या नहीं अनभिज्ञ थी मैं इस बात से किंतु आज उस गाछ का अद्भुत सौंदर्य मुझे भीतर तक आह्लादित कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं बाहर तो सूरज की छटा थी मेरे भीतर ही कहीं अंधकार था?
ऋतुएँ तो क्रमबद्ध आएँगी जाएँगी क्योंकि यह प्रकृति और ईश्वर द्वारा संयोजित व्यवस्था है हमारे लिए।
किंतु अपने हिस्से का बसंत तो हमें हर ऋतु में जुटाना होगा न?
बसंत की ही प्रतीक्षा क्यों? स्वयं प्राप्य व जुटाया हुआ बसंत क्यो नहीं?
जुटानी चाहिए हमें सौंदर्य बोध की कला बदरंग और हाशिए पर पड़ी वस्तुओं में, विकसित करनी चाहिए सृजनशीलता ताकि बसंत की सुगबुगाहट से पहले ही हम अपने एकाकीपन और एकांतवास में सहेज लें फूलों के अनगिनत रंग और तितलियों को तस्वीरों में, जैसे कि सर्दी की झड़ी से पहले घर में आग तापने के लिए लकड़ियाँ एकत्र की जाती हैं।
हुआ यूँ कि बसंत कभी लकदक कर उमड़ा ही नहीं मेरी तरफ़, स्वयं को ही ढाल लिया मैंने बाहर ओसारे में एक दूसरे पर ढलते, पछाड़ खाते गुलाब, पिटूनियाँ गजीनियाँ, डेन्थस, डाग फ्लावर के आग़ोश में।
स्वयं व्यवस्था जुटाई मैंने अपने हिस्से के बसंत को अपने क्रोड में बिठाने हेतु ऋतुओं की महत्ता से विरत होकर।
किंतु यह भी सत्य है कि पहाड़ों पर फ्यूली, बुरांस, मैदान में आडुओं और आम पर उतर आई मंजरी, गेहूँ की बालियाँ के परस्पर आलिंगन का सुर, गमकते गुलाबों की मुस्कराहट के रूप में बसंत की रंग-बिरंगी चादर हमारी आत्मा का गीत हैं। प्रकृति में बसंत की हनक है तो हमारे ह्रदय में भी उल्लास और स्पंदन की आहट है।
क्योंकि बाह्य सकारात्मक आवरण का स्वरूप ही हमारे अभ्यांतर प्रसन्नचित चेतना का अभिन्न हिस्सा हैं अतः बसंत का आग़ाज़ ऐसे ही होना चाहिए हम सभी के हृदय स्थलों में जैसे मायका छोड़कर पहली बार ससुराल की दहलीज़ पर क़दम रखती नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
सम्बंधित रचनाएँ

इगास पर्व उत्तराखंड - लेख - सुनीता भट्ट पैन्यूली

आस्था का महापर्व छठ - लेख - कुमुद शर्मा 'काशवी'

छठ पर्व - लेख - सुनीता भट्ट पैन्यूली

रावण, ज्ञान और अधर्म - लेख - सिद्धार्थ 'सोहम'

गांधी जी और स्वतंत्र भारत की स्त्री - लेख - सुनीता भट्ट पैन्यूली

हिंदी राजभाषा का उन्नयन और प्रसार - लेख - सुनीता भट्ट पैन्यूली
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर